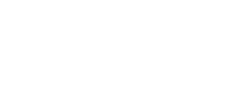कोई शख्स यूँ ही हर रोज मर रहा है!
हम मानना चाहते हैं कि हमारी हर सोच, हर बात, और हर कृत्य के जरिए हम अपना और अपनों का कल बदल रहे हैं। हमने मान लिया है की आज बदला नहीं जा सकता। जो आज से क्रोधित हैं उनसे हम क्रोधित हो जातें क्योंकि उनके सामयिक सवाल हमें अच्छे नहीं लगते।
लगें भी तो कैसे?
गंदगी हम देखना नहीं चाहते और बदबू झेलना हमारे बस का नहीं। खासकर जब मसला आस पास का हो। किसी सामयिक मुद्दे के मूल को अनदेखा करना या उसे टाल देना हमारी फितरत बन चुकी है। मुझे लगता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम औरों से तो अपेक्षाएँ रखना चाहते हैं पर स्वयं से नहीं।
क्योंकि आज को अनदेखा करना या टालना भी एक तरह का कर्म ही है, इस कर्म का भी फल होता है। फर्क बस इतना हैं कि उस फल को हमारी जगह कोई और भोगता है – हमसे दूर, वह जो हमारा नहीं। वह जो आकड़ा है – मर भी जाए तो हमें निजी तौर कर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी उधेड़बुन में लिखी गई है यह कविता।
कोई शख्स यूँ ही हर रोज मर रहा है!

कोई चौराहे पर खड़ा
सवाल कर रहा है,
कोई गुस्से में बड़ा
बवाल कर रहा है,
कोई जेल भर रहा है,
कोई जेब भर रहा है,
तो कोई बस सियासी
धक्कम-पेल कर रहा है।कोना कोई जिस्म का,
हर रोज सड़ रहा है;
कोई शख्स यूँ ही कहीं,
हर रोज मर रहा है!
कोई कारण बता रहा है
हर उठे बवाल का,
कोई जवाब सा खड़ा
हर उलझे सवाल का,
कोई कहता वो उजाला
इस अँधेरी रात का,
कोई सुल्झन का दंभ
हर बिगड़ी बात का।कोना कोई जिस्म का,
हर रोज सड़ रहा है;
कोई शख्स यूँ ही कहीं,
हर रोज मर रहा है!इंक़लाबी सपनों में
लिपटी हुई रातें,
नेक वादों, पक्के इरादों
की ख़ूबसूरत बातें,
उम्मीद-ए-उम्मीद में
चढ़ती उतरती साँसें,
इस देरी के दर्द में
अकड़ती जकड़ती आँतें।कोना कोई जिस्म का,
हर रोज सड़ रहा है;
कोई शख्स यूँ ही कहीं,
हर रोज मर रहा है।
कोना कोई इस जिस्म का,
हर रोज सड़ रहा है!