सत्येन्द्र – वृतान्त 2
***
इन्टरमीडिएट में अपने चुनिन्दा विषयों को पढ़ते हुए सत्येन्द्र ने जम कर मेहनत की। उसने ना सिर्फ इन विषयों को समझा अपितु एक व्यापक सामाजिक नजरिये से उन विषयों को उनकी पूर्णता में देखने का प्रयास भी किया। संगीत और नाटक के मोह ने उसे नुक्कड़ नाटक भी करवाए और देखते ही देखते वह जन अन्दोलनों का हिस्सा भी बन गया।
इन सब अनुभवों ने उसे इतिहास को एक नए नजरिये से देखने पर विवश भी किया। वह सोचने लगा की इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का क्यों होता है? लोग केवल ‘प्रजा’ ही क्यों होते हैं? लोगों के आन्दोलन केवल प्रजा के आंदोलनों तक सीमित क्यों हैं? अन्य बहुत कुछ भी तो घटा इन हजारों सालों में। भाषा, संगीत, संस्कृति, ज्ञान, खान पान, जीवन यापन, कला… यह सब इतिहास के किन कोनों में छिपे बैठे हैं? इन सब का इतिहास मुख्यधारा में क्यों नहीं हैं? लोक इतिहास केवल गोष्ठियों में बहस का मुद्दा क्यों है? उसे लगने लगा था की इन सवालों के उत्तर खोजने और स्वयं को विस्तृत करने के लिए उसे बहुत पढ़ना होगा। जगह जगह घूमना होगा। तरह तरह के लोगों से मिलना होगा। चर्चायें करनी होंगी। वाद विवाद करने होंगे। इसीलिए इन्टरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह नैनीताल की जगह दिल्ली चला गया। केंद्र का आकर्षण होता भी कुछ अलग ही है।
दिल्ली के रामजस कॉलेज में दाखिला लेते वक्त, पहले ही दिन उसकी मुलाक़ात स्नेहलता से हो गई। दोनों आस पास बैठे अपने फॉर्म भर रहे थे। सत्येन्द्र को कुछ दुविधा हुई तो उसने स्नेहलता से मदद माँगी। पता चला दोनों इतिहास में दाखिला ले रहे हैं। ऊपर से स्नेहलता देहरादून की निकली। फिर क्या था, पहाड़ प्रेम उन्हें फॉर्म भरने के बाद चाय की दुकान तक ले गया। चाय पर चर्चा के दौरान पता लगा की दोनों ने एक ही तरह के शौक पाल रखे हैं। इसलिए चाय से बात दोपहर के भोजन तक पहुँची और फिर दिल्ली भ्रमण की योजना में तब्दील हो गई। जुम्मे का दिन था और दोनों को निजामुद्दीन की दरगाह देखने की प्रबल इच्छा थी इसलिए दिन ढलने से पहले दोनों निजामुद्दीन पहुँच गए। कव्वाली के रस में डूबे हुए वे कब एक दूसरे में डूब गए उन्हें पता ही नहीं चला।

स्नेहलता ने बारहवीं की पढ़ाई देहरादून से की थी पर दसवीं तक वह भारत के कई छोटे बड़े शहरों में पली बड़ी थी। वह कर्नल गोविंद लाल की तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी। जब वह दसवीं में थी तब कर्नल साहब रिटायर हो कर देहरादून में बस गए। उनका मूल निवास पौड़ी जिले में था पर उन्हें अपने ‘मुल्क’ से कोई लगाव नहीं था। एक अछूत माने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बहुत कुछ देखा और झेला था उन्होंने। कई साल पहले देहरादून में मकान बना कर उन्होंने अपने माता पिता को भी यहीं बुला लिया था ताकि उन्हें अपने तथाकथित गाँव ना जाना पड़े। धर्म और जाति के आधार पर उभरती आधुनिक भारत की सभ्य बस्तियों में शायद उनके लिए अब भी जगह नहीं होती पर उनकी खुशकिस्मती थी की डिफेन्स कालोनी में चोटी नहीं सितारे देखे जाते हैं। ये बात अलग है की सितारों के बगैर वहाँ भी काम नहीं चलता।
स्नेहलता और सत्येन्द्र जल्द ही कॉलेज के रंग में पूरी तरह से ढल गए। वे दोनों कॉलेज की नाटक और संगीत मंडली का अभिन्न हिस्सा बन गए। सत्येन्द्र की ही तरह स्नेहलता को भी लोक कला और इतिहास में गहरी रूचि थी इसलिए वे छुट्टियों में घर जाने की जगह उन सब जगहों का भ्रमण करते जो उनकी वैचारिक खोज का हिस्सा थे। तीन सालों में वे भारत से सारे कोनों को छू आए। कई गोष्ठियों में गए। कई शोध पत्र लिखे। कई जगह नाटक किया। गाने गए। और जब जब मौका मिला, वे उन सब जगहों में भी गए जहाँ लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। लोगों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए उन्होंने अपनी निजी खोज को और परिपक्व किया।
कॉलेज खत्म होने तक वे जान चुके थे की उन्हें आगे पढ़ने के लिए मनपसंद कॉलेज ही नहीं अपितु मनपसंद गुरु की भी जरुरत है। गुरु की खोज उन्हें अमेरिका ले गई। उनका शैक्षिक व सामाजिक प्रोफाइल अच्छा था अतः उन्हें दाखिला भी मिल गया और स्कोलरशिप भी। बेटे के अमेरिका जाने की खबर से पन्तजी बेहद खुश थे। स्टेनफोर्ड में पढ़ना कोई मज़ाक बात थोड़े ही है।
स्नेहलता और सत्येन्द्र के मास्टर्स खत्म होने में देर नहीं लगी पर अभी पढ़ने समझने को बहुत कुछ बचा था इसलिए उन्होंने तय किया की वे वहीं अमेरिका में रह कर डॉक्टरेट भी करेंगे। पी.एच.डी. की खबर सुन कर पन्त मास्साब हवा में उड़ने लगे। वे सत्येन्द्र को बधाई पर बधाई दिए जा रहे थे कि तभी सत्येन्द्र ने अचानक बात बदलते हुए कहा, “बाबू, शादी करनी है।”
“शादी? किससे?”
“स्नेहलता, दोस्त है मेरी।”
“वहीं मिली क्या स्टेनफोर्ड में?”, बाबू ने उत्सुकता से पूछा।
“नहीं बाबू, रामजस से जानता हूँ। पर यहाँ भी हम साथ ही पढ़ते हैं।”
“पहाड़ी है?”
“हाँ!”
“पूरा नाम क्या हुआ?”
“क्या करोगे पूरा नाम जान कर बाबू। आप बस हाँ कह दो।”
“अरे, जात बिरादरी भी तो देखनी हुई ना बेटा। हालाँकि मैं जात पात नहीं मानता पर तुम्हारी माँ, दादी… वो लोग तो मानते हैं ना!”, पन्तजी ने बीवी और माँ के कंधों पर अपने पूर्वाग्रह की बन्दुक रखी और दाग दी।
“बाबू, आपका समाज उसकी जाति को निम्न मानता है। इसके आगे में इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता।”
पन्तजी को काटो तो खून नहीं। भगत सिंह की जयजयकार करने वाले भी अपने घरों में भगत सिंह नहीं चाहते। पन्तजी के लिए हाँ कहना मुश्किल था। कुमाउँ के उच्चतम कुल का लड़का अगर ऐसा करेगा तो कितनी बातें होंगी समाज में। उन्होंने यहाँ वहाँ की सुनाते हुए अपनी व्यथा बेटे से सामने रख दी, यह सब जानते हुए की सत्येन्द्र ना तो उनकी बात सुनेगा और ना ही मानेगा। बेटा नहीं माना। माँ रो दी पर बेटा फिर भी ना माना। इसलिए तय हुआ की शादी अमेरिका में ही होगी और वर वधु के माता पिता और भाई बहनों के सिवा और कोई नहीं बुलाया जाएगा शादी में। एक सुदूर पहाड़ी गाँव के लड़के की अमेरिका में शादी होना एक बड़ी बात है इसलिए पन्तजी मन ही मन कयास लगा रहे थे की इस बड़ी बात के पीछे शायद लड़की की छोटी जाति छुप जाएगी। वैसे बेटा अगर अमेरिका में नहीं होता तो पन्तजी यकीनन उसकी बात नहीं मानते। हदें भी तो आखिरकार औकात ही निर्धारित करती हैं।
समय अच्छा हो तो उसे गुजरने में देर नहीं लगती। सत्येन्द्र और स्नेहलता की शादी हुई ही थी की उनकी पी.एच.डी. भी पूरी हो गई। पन्तजी चाहते थे की बेटा विदेश में नौकरी करे। उसके वापस आने में और भी बहुत समस्याएँ थी जो ‘बच्चे नहीं समझ पायेंगे’ के चक्कर में चर्चा का विषय नहीं बनी। पन्तजी ने यहाँ वहाँ की सुना कर उन्हें वहीं रहने के लिए मनाने की कोशिश की पर बात नहीं बनी। सत्येन्द्र और स्नेहलता दिल्ली वापस आ गए। सत्येन्द्र रामजस में पढ़ाने लगा और स्नेहलता जे.एन.यू. में। दोनों ने तय किया की वे कॉलेज की कॉलोनी में न रह कर बीच शहर में कहीं रहेंगे ताकि संगीत और नाटक से उनका जुड़ाव बरकरार रहे। इस निर्णय के पीछे एक कारण यह भी था कि वे नहीं चाहते थे कि कॉलेज की दीवारें उनकी अभिव्यक्ति को किसी भी तरह से सीमित करें।
नाटकीय अभिव्यक्ति को नया रूप देने के लिए वे लोक परम्पराओं में डूबने लगे। नाट्य कला की पुरानी शैलियों पर शोध करने लगे। उन्होंने कई नए प्रयोग किए। इन प्रयोगों के मंचन के लिए उन्होंने धीरे धीरे एक सशक्त टोली भी खड़ी कर ली जो दिल्ली की सांस्कृतिक पटल का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। अब केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, और विदेशों से भी, लोग इन विधाओं को सीखने समझने के लिए उनसे जुड़ने लगे।
ऐसी ही एक खोजी थी मेनका राव। वह बँगलोर की रहने वाली थी और बंगाल की नाट्य परम्पराओं पर शोध कर रही थी। वह इस विषय पर एक फिल्म भी बनाना चाहती थी। उसका मानना था की सत्येन्द्र के दिशा निर्देशन में उसकी उड़ान और ऊँची हो जाएगी। इत्तेफाक की बात थी की सत्येन्द्र की खोज भी उसी दिशा में जा रही थी। वह टैगोर साहब की कथाओं के मंचन में बंगाल की पारम्परिक शैलियों का इस्तेमाल करना चाहता था। उसे लगा की मेनका के शोध से उसकी अपनी खोज को गति मिलेगी इसलिए उसने मेनका को अपनी टोली में शामिल कर लिया।
सत्येन्द्र अपने शोध के लिए एक महीने बंगाल जा रहा था। जब मेनका को यह पता चला तो उसने भी साथ जाने की इच्छा जाहिर की। पर सत्येन्द्र को यह मंजूर नहीं था, “पता नहीं कब कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या खाऊँ… ऐसे में किसी को साथ ले जाना मेरे लिए बन्धन सा हो जाएगा।”
“मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। वादा करती हूँ!”
“वादे से क्या होगा? ऊपर से जहाँ और जैसे में जा रहा हूँ, तुमको लेकर चिन्ता भी बनी रहेगी?”
“यह तो आपकी सोच है सत्येन्द्रजी। आप पिता का रोल निभाने की कोशिश नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक ही रहेगा।”
“मुझे जानती भी नहीं और मुझ पर पितृसत्ता की तोहमत लगा रही हो मेनका?”
“लगा तो नहीं रहीं पर आपकी सोच इशारा तो कुछ ऐसा ही कर रही है।”
सत्येन्द्र ने स्नेहलता की ओर देखा। स्नेहलता मुस्कुराई ओर बोली, “अपने ही बुने जाल में फँस रहे हो सत्येन्द्र बाबू। अब ले जाओ इसे। अगर तुमने मुझ पर अगले प्रोडक्शन का बोझ नहीं डाला होता तो मैं भी चलती। फिर क्या करते? मुझे भी मना कर देते?”
सत्येन्द्र चुप हो गया। कमरे के किनारे रखी अलमारी से उसने तीन काँच के गिलास और एक व्हिस्की की बोतल निकाली, छोटे छोटे पेग बनाए, गिलासों में पानी भरा, और उनको ट्रे में रख कर स्नेहलता और मेनका के पास ले आया। तीनों ने अपने अपने गिलास उठाए, “जय हो!” कहते हुए चियर्स किया और एक ही घूँट में पूरा पेग गटक गए। गिलास को टेबल पर जोर से रखते हुए सत्येन्द्र बोला, “नई खोजी यात्रा के लिए!” स्नेहलता ने भी उसका अनुमोदन किया, “नई खोजी यात्रा के लिए!” और देखादेखी, थोड़ा झिझकते हुए, मेनका ने भी अपना गिलास टेबल पर पटक सा दिया।
“तोड़ोगी क्या?”, सत्येन्द्र बोला। मेनका हँस दी। स्नेहलता मुस्कुराते हुए बोली, “सीख जाएगी! जल्द सीख जाएगी! ऐसे काम सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता!”

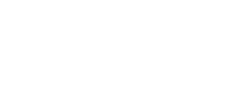













कहानी रोचक है मगर तूफानी गति से भाग रही है। चूँकि दोनों किरदारों को पहाड़ ने मिलाया है इसलिए आगे उसी जीवन के अंतर्विरोध उभरने चाहिए, संयोगात्मक नहीं, आज के यथार्थ के। इतनी जल्दी क्या है, ठहर कर पहाड़ लाकर उन्हें यहाँ की कड़वाहट से तीखे ढंग से रू-ब-रू कराइए, शायद इससे यह फ़िल्मी होने से बच जाए।
जी शुक्रिया। इस भाग में कहानी भाग रही है, शायद ज्यादा ही तेज भाग गई 🙁 फ्लैश्बैक जैसा कुछ दर्शाने का प्रयास कर रहा था।